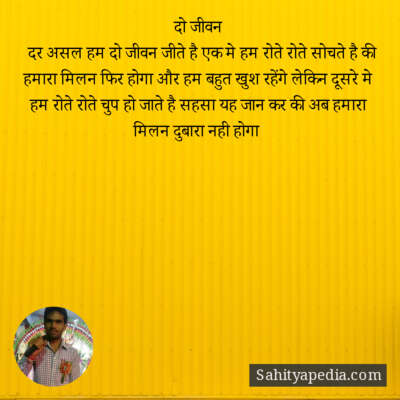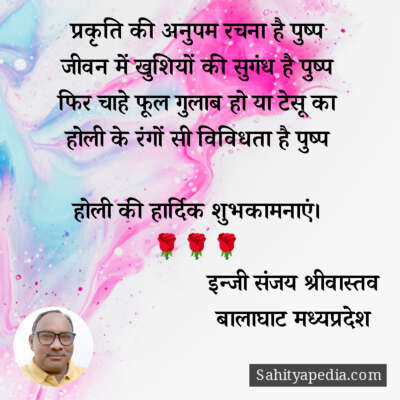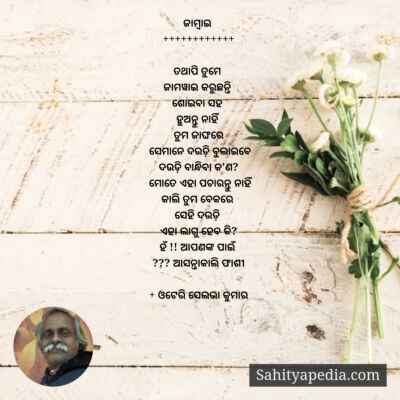सोच रहा हूँ जीवन पर इक गीत लिखूँ मैं
ईर्ष्या,द्वेष,कलह में लिपटी
सच्ची-झूठी प्रीत लिखूँ मैं
सोच रहा हूँजीवन पर इक गीत लिखूँ मैं।
माँ जीवन का मूर्त रूप अंतर में ढाला करती है
कितनो के ही स्वप्न निरंकुश गर्भ में पाला करती है
थक जाए तन तो नयनों में नींदें पैदा होती है
जन्म नहीं लेता शिशु बस उम्मीदें पैदा होती हैं
वीणा के तारों में झंकृत
कर्कश सा संगीत लिखूँ मैं
सोच रहा हूँ जीवन पर इक गीत लिखूँ मैं।।
दब जाता है प्यारा बचपन उम्मीदों की बोझ तले
मिलते हैं कितने ही ताने बिस्तर पर हर रोज गले
तितली,जुगनू,बाग-बगीचे,पोखर,पानी भूल गए
रोया फूट-फूट मन मेरा जब बच्चे स्कूल गए
हँसते फूल बिखेर चली जो
वही भयंकर शीत लिखूँ मैं
सोच रहा हूँ जीवन पर इक गीत लिखूँ मैं।।
धीरे-धीरे उम्र चरम से खुद ही ढलने लगती है
दुनियादारी की बातें आँगन में चलने लगती हैं
रुग्ण हो तन तो व्यंजन भी जिह्वा को फीके लगते हैं
बीवी-बच्चे, रिश्ते-नाते स्वप्न सरीखे लगते हैं
यही सोचता है मन पागल
अब किसको मनमीत लिखूँ मैं
सोच रहा हूँ जीवन पर इक गीत लिखूँ मैं
अंतकाल जब उड़े मुखौटा मात्र बेबसी होती है
हो अमीर की या गरीब की चिता एक सी होती है
मायावी इस दुनिया में जब कालचक्र चल जाता है
क्षण भर रुकती नहीं आत्मा नश्वर तन जल जाता है
मृत्यु नया इक जीवन है
फिर क्यों होकर भयभीत लिखूँ मैं
सोच रहा हूँ जीवन पर इक गीत लिखूँ मैं