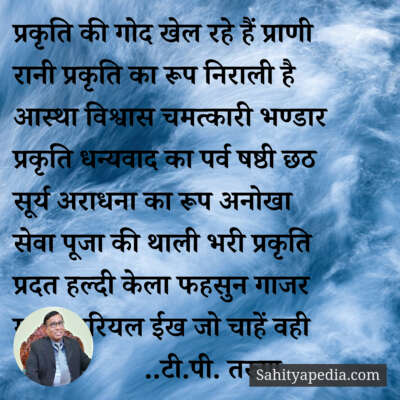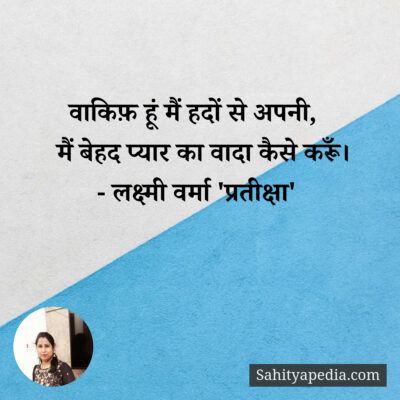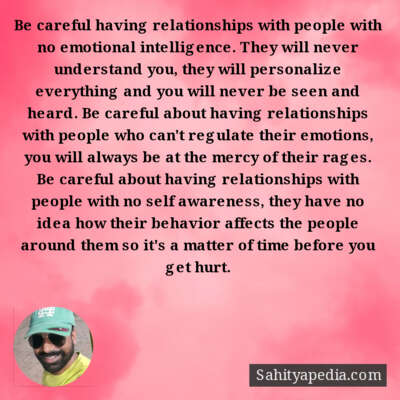वो आंगन ढूंढ रहा हूं
आज फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ,
जो न जाने कहाँ गुम हो गया है।
बहुमंजिल कंक्रीट जंगल में,
या ऊंचे फ्लेटों में लुप्त हो गया है।
वह आंगन के बीच की रंगोली,
वो तुलसी और मर्वे का कमला,
वो आंगन में चिड़ियों का पानी,
वो गौरय्या की प्यारी चहचाहट,
वो आँगन में दादी का फटकारना,
वो दादा जी का फिर पुचकारना।
आज फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ,
जिसपर गाय के गोबर से लिपाई है,
जहां दिवाली रात को तारे आते हैं।
जहां शादी की सतरंगी सजावट है,
जहां घर बार की औरतों की हँसी है।
जहां आँसुओं भरी कन्या विदाई है,
जहां देते सुबकते माँ बाप दिखाई हैं।।
आज फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ,
जहां वर्षा की बूंदों का आनंद है,
जहां खेत से लाई गई वह सीपी है।
जहां पलिंदे में रखे घड़े दिखते हैं,
जहां नहाये पानी से पौधे सींचते हैं।
जहां पलिण्डैं में मरवे की महक है,
जहां सहेली कन्याओं की चहक है।
आज फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ।
जहां आँगन के आगे वो बाखल है,
जहां कोने में रखे मूसल-औखल है।
जहां बाखल में पशुओं के ठांण है,
जहां बच्चों के खेलने का मैदान है।
जहां चारपाई पर बतलाते चाचा है,
जहां शान से बनाता कोई मांजा है।
आज फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ।।
हो सके तो माफ करना मेरे बच्चों,
नहीं ढ़ूंढ़ सका फिर वो आँगन,
नहीं दिखा सकूँगा तुम्हें वो आँगन,
‘पृथ्वी’ नहीं दे पाएगा बच्चों तुम्हें,
वो संस्कृति भरा वो अपना आँगन।
क्योंकि फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ,
आज फिर वो आंगन ढ़ूंढ रहा हूँ।।