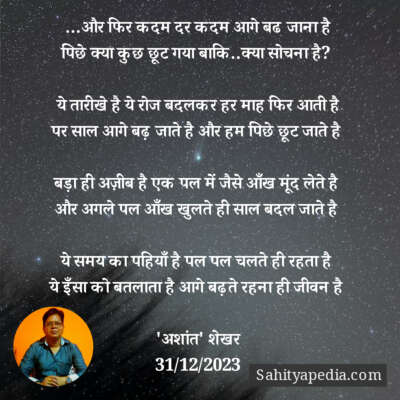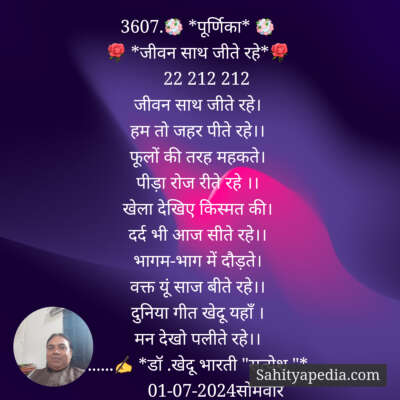यथा_व्यथा

संवाद करने भर के लिए स्त्री,
क्यों आखिर शब्दावली तलाशती है;
जब बिखर जाते हैं अर्थ तो,
खुद पर ही लगाम लगाती है;
सुन लो तुम ज्ञात कर सको अगर,
तो एक बार कोशिश करके देख लो,
एक चहकती अठखेलियां करती स्त्री
सब पाकर भी…क्यूँ मौन हो जाती है,
आखिर क्यों बरसों से मौन है,
उस चंचल स्त्री के अंतर्मन की,
सोई हुई बेबस इच्छायें;
जिन्होंने आखिर थाम लिया
कुछ मजबूरियों का साथ;
और कितना नेह बड़ा लिया है;
आभासी ज़िम्मेदारियों का दामन थामकर;
रोज़ जुझारू हो जाती है…..,
बरसती उम्मीदों का कल्पवृक्ष बन कर;
परिपक्व होती जाती है….
अपनी बढ़ती उम्र से पहले ही…!
तार्किक अभिव्यंजनाएं भी उसकी
क्यों उसे दिशाविहीन बना जाती है;
और सिंहनी सी दहाड़ भी कई बार
सामाजिक कुचक्र में दब जाती है,
क्यूँकि उसके मुखर होने से भी,
वो दोराहे पर आ ही आती है;
अँधेरे में घुसकर ख़ाक भी छाने
फिर भी कहाँ सराही जाती है;
मचलती है बिन पानी मीन सी
गरम रेत में पैर झुलसाती है;
कमर कसकर मेहनत से भी कब,
मनमाफ़िक जगह बना पाती है;
स्त्री के दायरे…निहित हैं;
सदियों से बड़ी बातों में,
दुनिया पलटवार कर उलझाती है;
जोर शोर से डंके पिट रहे हें,
बराबरी के हक़ पा जाने के उसके,
लेकिन फिर भी कहाँ बराबरी की,
तुमसे वो हिम्मत जुटा पाती है;
भ्रम है सब कुछ पा लिया उसने,
फिर क्यूँ एक गहरे मौन में लौटकर,
वो फिर गुमशुदा हो जाती है,
पर विस्तृत प्रतिशत है ये यथा व्यथा,
जो अनंतकाल से दुहराई जाती है;
संवाद करने भर के लिए स्त्री
क्यों आखिर शब्दावली तलाशती है
जब बिखर जाते हैं अर्थ तो
खुद पर ही लगाम लगाती है
सुन लो तुम ज्ञात कर सको तो,
एक बार कोशिश करके देख लो,
एक चहकती अठखेलियां करती स्त्री,
सब पाकर भी क्यूँ मौन हो जाती है;
©anitasharma