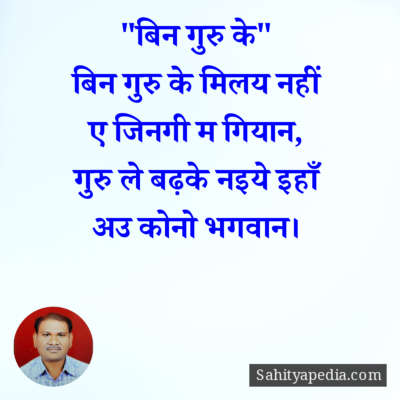महानगरीय जीवन
महानगर में गुमशुदा, है मेरी पहचान।
हिस्सा हूँ बस भीड़ का, हर कोई अनजान।।
घर से बेधर हो गई, दो रोटी की चाह।
जंगल मानव का यहाँ, अंजानी-सी राह।।
भीड़ भरी शहरी सड़क, सभी चीज गतिमान।
शोर प्रदूषण है बहुत, सूख गई है जान।।
महानगर बिखरा हुआ, तन्हा हर इंसान।
मकान का नंबर बना, बस अपनी पहचान।।
है मशीन-सी जिन्दगी ,मिले नहीं आराम।
सुबह सूर्य थकता यहाँ, बदमिजाज-सी शाम।।
शोर-शराबे में दबी, खुद अपनी अावाज।
महानगर में गंदगी, धुन्ध-धुआँ का राज।।
महानगर में तेज है, जीवन की रफ़्तार।
चका-चौंध में हैं दफन, रिश्ते-नाते प्यार।।
शुद्ध हवा पानी नहीं, दम-घोटू माहौल।
पहनावे को देख कर, जाती आत्मा खौल।।
महानगर में हो रहा, पश्चिम का अवतार।
होती गरिमा प्रेम की, यहाँ देह विस्तार।।
रोने वाला भी नहीं, पत्थर जैसे लोग।
हँसना रोना भूलकर, देखें केवल भोग।।
शहरों में बीमार – सी, लगती सूर्य प्रकाश।
यहाँ प्राकृतिक नाम पर, बचा सिर्फ आकाश।।
दया-धर्म ममता नहीं, बढ़ी मार-अरु-काट।
मानव जीवन मूल्य की, लगी हुई है हाट।।
गर्म हवाओं का सभी, पहने हुए लिबास।
महानगर में लोग का, मरा हुआ अहसास।।
सहज खींच लाती यहाँ, भौतिक सुख की खोज।
आपा-धापी हर तरफ, लगी हुई है रोज।।
महानगर कहते जिसे, होता नहीं महान।
इमारतें ऊँची मगर, निम्न कोटि इंसान।।
महानगर के द्वार पर, लिखा एक संदेश।
आने वालों छोड़ दो, मानवता का वेश।।
महानगर को देखकर, मन हो गया उचाट।
लौट चले फिर गांव में, देख रही है बाट।।
– लक्ष्मी सिंह