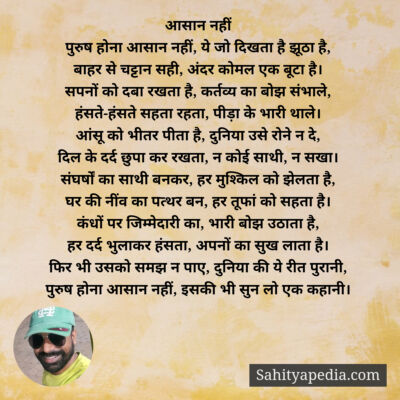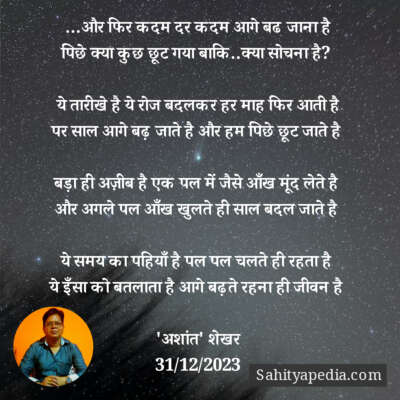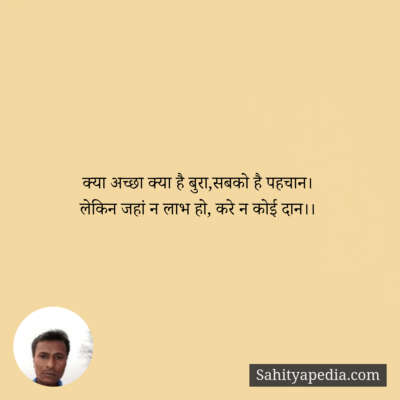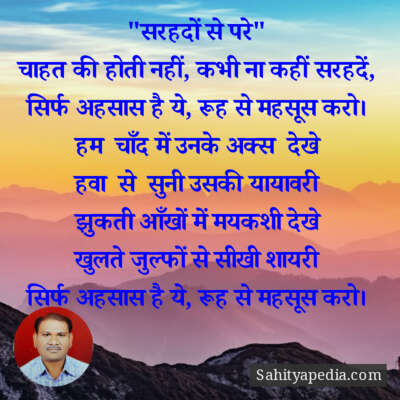मर्ज
आलिंगन भर कर लेते तो ,तेरी खुशबू देह में होती।
नाहक ही विरहा झेला हूं,जीवन को संतत्पित मानो।
मैं आकाश प्रेम लुटाता,तेरे नाम पर गीत बनाता।
किंतु अब आहें लिखता हूं,मुझको पत्थर वेदित मानो।
तितली का फूलों पर आना,देख के लगता बड़ा सुहाना।
किंतु सहमी आंखों को अब,तेरे दीद का तृष्णित मानो।
वैशाखों में तुम पुरवाई ,बन क्षण भर उर त्रास बुझाई।
नव पल्लव के रंगों को ,अब अच्छा है जर्जित मानो।
भले हकीक़त में दूरी है किंतु उर में छवि तुम्हारी।
वक्त बदल चुका है किंतु अब भी मुझको अर्पित मानो।
दीपक झा “रुद्रा”