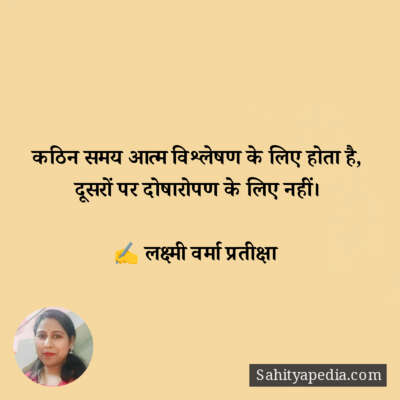दिन अभी ढला नहीं – लघुकथा
“कितने साल गुजर गए सुधा, लेकिन ज़्यादा नहीं बदला हमारा गाँव। बस कुछ आधुनिकता की निशानियों को छोड़; वही बाग-बगीचे और वही हरे-भरे रास्ते।” शाम की सैर के बीच छाई चुप्पी को भंग करते हुए उमाशंकर जी ने पत्नि से बात शुरू की।
“सही कहा आपने। कुछ बगीचों की बाड़ जरूर टूटी-फूटी लकड़ियों की जगह ‘मेटल’ की खपचियों से बन गयी है, पहले से सुंदर और ज़्यादा मजबूत।” सुधा ने सामने नजर आते बग़ीचों की बाड़ के उस पार लहलहाती फसल को निहारते हुए उत्तर दिया।
. . . बरसों बाद लौटे थे वे गाँव। बहुत पहले ही अपनी ज़िद के चलते अपना संयुक्त परिवार छोड़ बच्चों को लेकर विदेश चले गए थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि गाँव के देहाती-अनपढ़ माहौल में उनके बच्चे सांस लें। और फिर समय गुजरता गया, उन्होनें अपने बच्चों को शिक्षित और आधुनिक नागरिक के साथ सफल इंसान भी बनाया लेकिन शायद उचित संस्कार नहीं दे पाए। परिणामतः आज फिर वह अपने गाँव में लौट आए थे, नितांत अकेलेपन को लेकर।
“मैं जानता हूँ सुधा, तुम्हारे लिए गाँव में रहना कठिन है लेकिन बच्चों से मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूँ पर उनका बार-बार तुम्हारा अपमान करना, यह बर्दाश्त नहीं होता था। ख़ैर, उन्हें सही संस्कार नहीं दे सके; ये दोष भी तो हमारा ही है।”
“आप ऐसा न कहें और परेशान भी न हों। मुझे यहाँ कोई दिक़्क़त नहीं होगी।” पति की बात का प्रत्युत्तर देते हुए वह कहने लगी। “सच तो ये है कि मैं सारा जीवन यही समझती रही कि उच्च शिक्षा और आधुनिक सभ्यता से ही हम संतान को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। लेकिन अब जाकर समझी हूँ कि संस्कार तो प्रकृति के वो बीज होते हैं जो परिवार के बुजुर्गों और अपनों के सानिध्य-प्रेम में ही पैदा होते हैं। काश कि हमने अपने बच्चों की परवरिश यही परिवार के बीच रहकर की होती, तो जीवन की ढलती सांझ में हम अकेले नहीं होते।”
“सुधा, बीता हुआ समय तो लौटकर नहीं आता लेकिन हम चाहें तो अतीत का प्रायश्चित कर सकते हैं।” उन्होंने अपनी नजरें पत्नी की ओर जमा दी।
“कैसे. . .?”
“सुधा!” पत्नी की प्रश्नवाचक नजरों को निहारते हुए उनकी आँखों में एक विश्वास था। “हमारे समाज में और भी बहुत से परिवार बिखरे हुए हैं या बिखरने की कगार पर है, जिन्हें हम चाहें तो. . .!”
“हाँ क्यूँ नहीं, इससे बेहतर हमारे जीवन का आख़िरी पड़ाव और क्या होगा?” पति की अधूरी बात पर सहमति की छाप लगाते हुए सुधा ने मुस्कराते हुए पति का हाथ थाम लिया।
विरेंदर ‘वीर’ मेहता