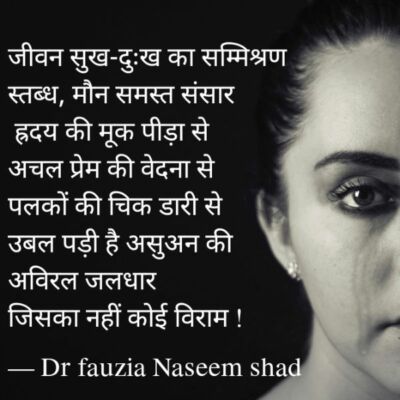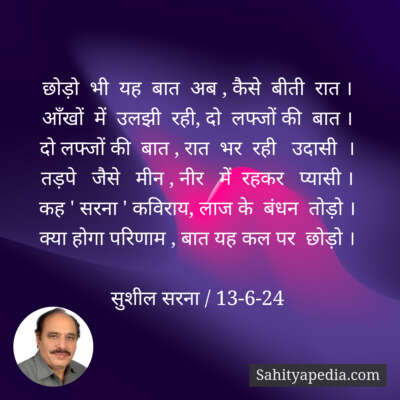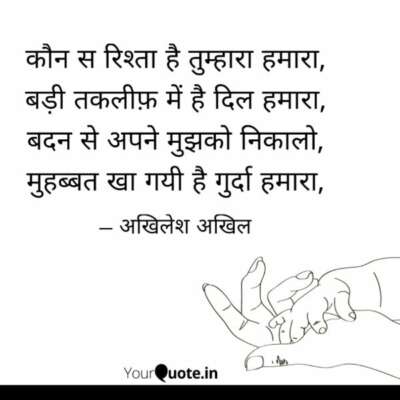ज़िंदगी
द्वार खड़ी थी इक दिन वो, बनठनकर मुस्कान सजाकर
बेतरतीब सी बाहर आकर, देखा था मैंने आँखे मलकर
हाथ थामकर बोली हाय, भूल गई तू मुझको क्योंकर
देख रही थी अपलक मैं, बातें उसकी निश्छल सुनकर
खूब हँसाया मुझको उसने, बचपन मेरा याद दिलाकर
तरुणाई की रुचिर सलोनी, कनबतियों को दोहराकर
हाल बुरा क्यों तेरा ऐसा, हौले से बोली गाल को छूकर
सुन्दर मुख में सलवट कैसी, पूछा उसने नेह से भरकर
खुली हवा में खींच ले गई, जबरन मेरी बाँह थामकर
बारिश में फिर मुझे भिगोकर नाच उठी थी घूम घूमकर
सौगात में फुरसत के पल देकर, गीत लबों पर ठहराकर
झलमल नैनों से जादू सा कर, अरमानों से झोली भरकर
खुशियों का अंबार लगाया, प्रीत की चूनर लहराकर
मन की निर्जल धरती पर, चाहत की फुहारें बरसाकर
सम्मोहित सा मुझे कर गई, दीप आस का दिखलाकर
चैतन्य मुझे वो पुनः कर गई, जीवन अमृत बिखराकर
जब पूछा मैंने नाम था उसका, खूब हँसी थी इठलाकर
बोली मुझसे, मैं हूँ ज़िंदगी, जीती है तू जिसे भुलाकर
डाॅ. सुकृति घोष
ग्वालियर, मध्यप्रदेश