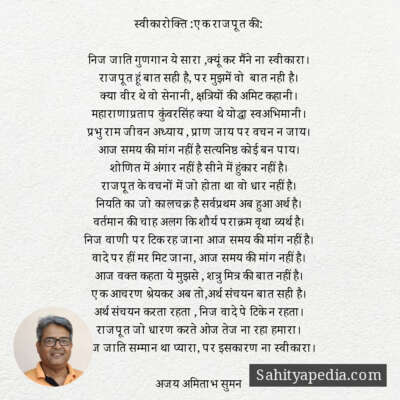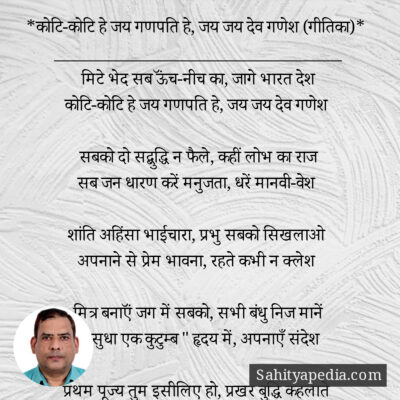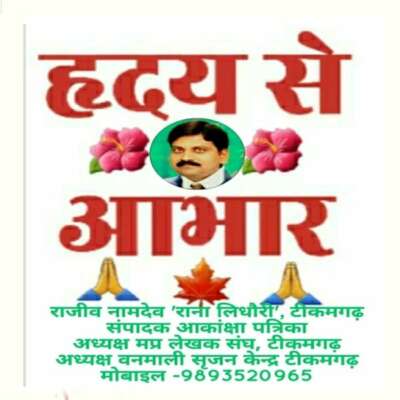जब सांझ ढल चुकी है तो क्यूं ना रात हो

सजदे
के लिए उठता है
ये दस्त हज़ार बार
पर सोच के रुक जाता हूँ
किसको करूं सलाम
उनके आने का ग़ुमां सा होता है
न जाने कितनी बार
पर सोचता हूँ हर बार
शायद हसीं ख्वाब ना हो
मानी थीं मन्नतें
जो उनके
अहले कर्म की
अब तो है यही इल्तज़ा
की वो ख़ुदा को ना याद हों
है गर्दिशे अय्याम
कुछ रास यूं आया
आरज़ू है कि
और कोइ मुकां ना हो
उम्मीदों कि लाश पे
खड़ी है ये
जरज़्रे जिंदगी
है कौन इसका वाली
ना मालूम
कब रूह फ़ना हो
जद्दोजहद क्या करे
“घायल” अब मौत से
जब सांझ ढल चुकी है
तो क्यूं ना रात हो