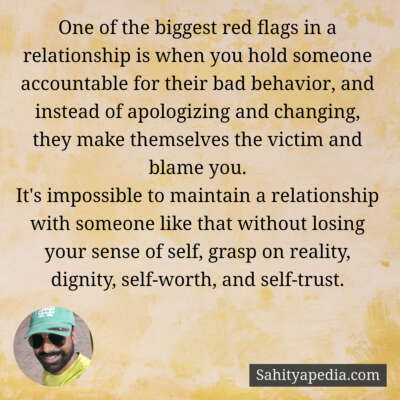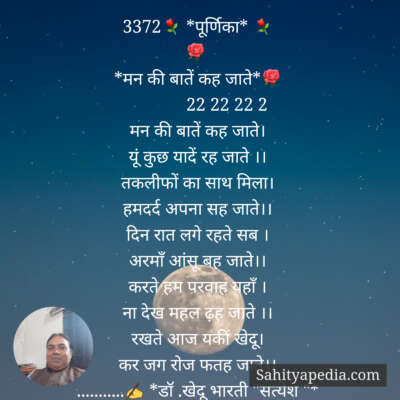ग़ज़ल एक प्रणय गीत +रमेशराज

ग़ज़ल का अतीत एक प्रणय-गीत, महबूबा से प्रेमपूर्ण बातचीत’ के रूप में अपनी उपस्थित दर्ज कराते हुए साहित्य-संसार में सबके सम्मुख आया। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ‘मद्दाह’ का शब्दकोष देख लीजिए, उ.प्र. हिन्दी संस्थान की प्रामाणिक शब्दकोषीय पुस्तक टटोल लीजिए, या ‘नालंदा अद्यतन शब्दकोष’ का अवलोकन कीजिए, इन सबके भीतर ग़ज़ल शब्द का ‘अर्थ प्रेमिका से प्रेमपूर्ण बातचीत’ ही इसके अतीत का साक्षी बनकर खड़ा है। वह चीख-चीख कर कह रहा है कि ग़ज़ल की खमदार जुल्फें हैं, आँखों में काजल से कँटीलापन है, अधरों पर प्रेमी से मिलने का आलाप है। हाथों पर मेंहदी का रचाव है, पाँवों में प्रेमी को रिझाने के लिये महावर से रचाव है। हिरनी जैसी चाल है। मस्ती है, धमाल है। ग़ज़ल प्रेमी के लिये या तो प्रेमिका से मिलने का आमंत्राण है या निरंतर मिलते रहने का प्रण है। ग़ज़ल का रूहानी रूप भी आशिक और मासूक का मायाजाल है। ग़ज़ल रति और कामदेव-के मिलन की प्रेमकथा है। ग़ज़ल का हर रूप-स्वरूप सिर्फ और सिर्फ ‘प्रणय निवेदन’ में रचा-बसा है।
ग़ज़ल एक निश्चित शिल्प ;शे’र, रदीफ, काफियों, मतला और मक्ता के साथ-साथ एक निश्चित बहर में अपनी नाजुक-बयानी के लिये जानी और मानी जाती है। लेकिन आज के कथित ग़ज़लकार को इसके इस रूप को प्रयोग में लाते हुए भी इसी रूप पर शर्म भी आती है। वह ग़ज़ल के इस प्रेम-रूप को मारना चाहता है। मतला, मक्ता से मुक्ति के साथ-साथ इसकी बहरों के पेट में चाकू उतारना चाहता है। इसकी आत्मा ‘प्रणयात्मकता’ के सीत्कार को आम आदमी के चीत्कार में बदलकर इसमें जनवादी चरित्र फिट कर हिट होना चाहता है। हिट होने की यह गिटपिट भले ही ग़ज़ल के शास्त्रीय पक्ष के अनुकूल न हो, लेकिन वह इस तरीके से सामाजिक सरोकारों के फूल खिलाना चाहता है। वह अपनी एक ही ग़ज़ल के कुछ शे’रों में थिरकती चितवन के वाण छोडता है, प्रेमिका से आलिंगनबद्ध होता है, रति और कामदेव की तस्वीर खींचता है तो उसी ग़ज़ल के अन्य शे’रों को जनपीड़ा से जोड़कर, महान हो जाना चाहता है। ग़ज़ल के भीतर का सीत्कार जब चीत्कार का भी आभास देने लगता है तो ग़ज़लकार के ग़ज़ल कहने या लिखने, पर एक उपहास, अट्टहास की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। और फिर सवाल उठाता है कि क्या ‘प्रेमिका को बाँहों में भरने का जोश’ और ‘कुव्यवस्था से पनपा आक्रोश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या चुम्बन और क्रन्दन का अर्थ एक ही होता है?
‘सीत्कार’ और चीत्कार, ‘प्रेमिका को बाँहों में भरने के जोश’ और कुव्यवस्था से पनपे सामाजिक आक्रोश तथा चुम्बन और क्रन्दन का क्या एक ही अर्थ होता है? दुर्भाग्य यह है कि आज का मानसिक रूप से बीमार ग़ज़लकार इन चीजों में भेद करने को तैयार नहीं है। अशुद्ध मतलों या लुप्त रदीफ-काफियों से युक्त कथित ग़ज़ल के प्रति उसका विश्वास यह है कि वह श्रेष्ठ ग़ज़ल कह रहा है | उस पर दम्भ यह कि उसके इस कर्म को श्रेष्ठ कर्म माना ही नहीं, सराहा भी जाये। ऐसे ग़ज़लकार ग़ज़ल की बहर के विधान को जानते ही नहीं हैं, इसलिये उसमें हिन्दी छन्दों को घुसेड़ रहे हैं। हिन्दी में हिन्दी-छन्दों की मात्राएँ गिराकर, सुकर्म नहीं कुकर्म करने में जुटे हैं। ग़ज़ल का हर शे’र पूर्ण होता है ठीक ‘दोहे’ की तरह। किन्तु इस व्यवस्था को तोड़कर ग़ज़ल को गीत जैसा रूप देकर वह मगन है। ग़ज़ल अपने इस आत्मरूप और विकृत शिल्प पर आँसू बहा रही है। लेकिन ग़ज़लकारों को अपने इस कुकर्म पर जरा भी शर्म नहीं आ रही है।
ग़ज़ल के इन कथित महान रचनाकारों, परम विद्वानों, अति ज्ञानियों को ग़ज़ल के प्रति किये गये कुकर्म को लेकर आशंका न हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ये विद्वान अनेक शंकाओं से भी घिरे हैं। तभी तो इस विकृत रूप को नये-नये नाम देने की कोशिश में लम्बे समय से जुटे हैं। कोई इन्हें ‘गजलिका’ कहता है तो कोई ‘ अग़ज़ल’, कोई इसे ‘गीतिका’ नाम देना चाहता है तो कोई ‘मुक्तिका’। कोई इसे ‘बाल ग़ज़ल’ पुकार रहा है तो कोई ‘दोहा ग़ज़ल’। कोई ‘हिन्दी ग़ज़ल’ के रूप में इसकी स्थापना करना चाहता है तो कोई ग़ज़ल के नीचे के नुक्ते हटाकर इसे ‘नुक्ताविहीन गजल’ के रूप में हिन्दी की अमूल्य विरासत बना रहा है। कुल मिलाकर ग़ज़ल के नियमों-उपनियमों, शास्त्रीय पक्षों को पछाड़कर, ग़ज़ल को जड़ों से उखाड़कर ऐसे कथित ग़ज़लकार ग़ज़ल पर विशेषांक-दर-विशेषांक निकाल रहे हैं, अपने ग़ज़ल संग्रहों की ऐसी भूमिकाएँ स्वयं लिख रहे हैं या अन्य ग़ज़ल-भक्तों से लिखवा रहे हैं और ग़ज़ल के सुधी पाठकों को समझा रहे हैं कि ग़ज़ल अब ग़ज़ल की नकल नहीं रही। इसकी नयी शकल हम गढ़ रहे हैं, ग़ज़ल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन इसी बदले रूप को स्थापित करके मानेंगे।
आज की ग़ज़ल यदि ग़ज़लपन की सारी शर्तों को पूरा कर रही होती तो उसे ‘सजल’,‘ग़ज़लिका’, ‘अगजल’ गीतिका, मुक्तिका, दोहा ग़ज़ल, बाल ग़ज़ल, व्यंग़ज़ल, आजाद ग़ज़ल, अवामी ग़ज़ल, ‘नुक्ताविहीन गजल’ आदि-आदि नये नाम देने की आवश्यकता न पड़ती। ‘गीतिका’ एक चर्चित छंद है, फिर ये ‘गीतिका’ क्या है? मुक्तिका किस चीज से मुक्त होना चाहती है? अगजल जब ग़ज़ल है ही नहीं तो इस नाम का औचित्य क्या? आज यदि बहर की हत्या कर ‘दोहा ग़ज़ल’ आयी है तो क्या ‘दोहा ग़ज़ल’ के समान छन्द के आधार पर गीतिका, हरिगीतिका, चैपाई, सोरठा आदि ग़ज़ल के रूप सामने आने चाहिए या आयेंगे? आज यदि ‘बाल ग़ज़ल’ लिखी गयी है तो क्या भविष्य में उम्र को ध्यान में रखकर किशोर, किशोरी, युवक-युवती, प्रौढ़ा, वृद्ध-वृद्धा ग़ज़ल भी लिखी जायेंगी? ठीक यही स्थिति अवामी ग़ज़ल, आजाद ग़ज़ल की है? अवामी ग़जल नाम यदि सही है, तो नेता ग़ज़ल, अफसर ग़ज़ल, उद्योगपति ग़ज़ल, सेठ-ग़ज़ल की शकल थी देखने को मिलेगी? आज ग़ज़ल में यदि ग़ज़ल के नियम उपनियम आजाद हैं तो इस कथित आजादी में क्या इसके शास्त्रीय स्वरूप की हत्या नहीं?
ग़ज़ल के शास्त्रीय आधार की हत्या करने वाले ऐसे ग़ज़लकार इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने में तो अपने हलक को सूखा कर लेते हैं, किन्तु सवाल जब हिन्दी साहित्य की नूतन विधा तेवरी का आता है तो ग़ज़ल के यही कथित पक्षधर, दम्भी-अहंकारी विद्वान तेवरी के प्रति मुखर ही नहीं होते, प्रहार और वार की मुद्रा में आ जाते है और चीखते-चिल्लाते हैं कि-‘‘ तेवरी को ग़ज़ल के शिल्प में क्यों लिख रहे हो। तेवरी अपरिपक्व मस्तिष्कों की उपज है, खालिस्तान बनाने की माँग है। ग़ज़ल का अधकचरा अनुकरण है। आज यदि तेवरी आयी है तो कल इसका पीछा घेवरी और पेवरी भी करेंगी।’’ आदि-आदि”।
तेवरी के शिल्प पर ग़ज़ल की नकल के आरोप ऐसे ग़ज़ल के अतिज्ञानी थोप रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि जब किसी रचना का कथ्य बदलता है तो उसी के साथ शिल्प भी परिवर्तित हो जाता है। शिल्प भी उसी राग को गाता है, जो कथ्य को सुहाता है। देखा जाये तो कथ्य और शिल्प में अधूरे प्रकार से नहीं, पूरी तरह समानुपाती नाता है। शिल्प काव्य का वह साधन है जिसके माध्यम से विचार के द्वारा बने भाव, अनुभाव के रूप में प्रकट होते हैं। काव्य में अन्तर्निहित विचार जिस प्रकार का है, वह उसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा भाषा के उसी रूप को ग्रहण करती है, जिसके माध्यम से पाठकों, दर्शकों तक सहज, सरल और सार्थक तरीके से सम्प्रेषित हो सके। मसलन-यदि किसी कविता में रौद्ररस को प्रकट किया गया है तो उस रस की शब्दावली में वही शब्द आयेंगे या आते हैं, जिनमें तल्खी, ललकार, मार, फटकार, वार, संहार, प्रतिकार, दुत्कार, गर्जना आदि हो। यदि कविता शृंगार रस की होगी तो उसकी शब्दावली रौद्ररस के शब्दों के ठीक विपरीत ऐसे शब्दों को चयनित करेगी जिनमें प्यार, अभिसार, चुम्बन, आलिंगन, सीत्कार, मिलन आदि का स्पर्श हो। ऐसा कदापि नहीं होगा कि कविता रौद्ररस की हो और उसकी शब्दावली में पायल की खनक, मैंहदी और महावर का रचाव, मिलन का चाव शाब्दिक स्थान पा सके। इसका सीधा अर्थ यह है कि तरह-तरह के विचारों से उत्पन्न भाव भी तरह-तरह के होते हैं और इन भावों के बदल जाने पर उनसे उत्पन्न अनुभावों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है, भाव बदलने पर वह माध्यम भी बदल जाता है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विचार और भाव अर्थात् काव्य का आत्मरूप कथ्य यदि परिवर्तित होता है तो काव्य के शिल्प का एक पक्ष यदि रस बदलता है तो दूसरा पक्ष उसकी भाषा शैली भी खुद-ब-खुद बदल जाती है।
लेकिन ग़ज़ल फोबिया के शिकार हमारे माननीय ग़ज़लकार हैं कि वे ग़ज़ल के आत्मरूप [विचार और भाव] जिसमें शृंगार रस का ही समावेश होना चाहिए, उसे बदलकर उसमें व्यवस्था के प्रतिकार, पीडि़त की चीत्कार, सामाजिक सरोकार, आम आदमी के अभाव-घाव, नैतिक पतन, यहां तक कि कथित जनवादी चिन्तन को उसमें ठूँस रहे हैं। ग़ज़ल की प्रणयात्मक भाषा शैली को बदलकर उसे व्यवस्था के सताये लोगों की क्रन्दन शैली बना रहे हैं।
इस सुकृत्य से ग़ज़ल के कथ्य में जो बदलाव आया है, जो विरोध रस का स्वर मुखरित हुआ है, उसे न तो पहचान पा रहे हैं, और न इस कथ्य और शिल्प के बदलाव को नया सार्थक नाम देने का प्रयास कर रहे हैं।
-रमेशराज