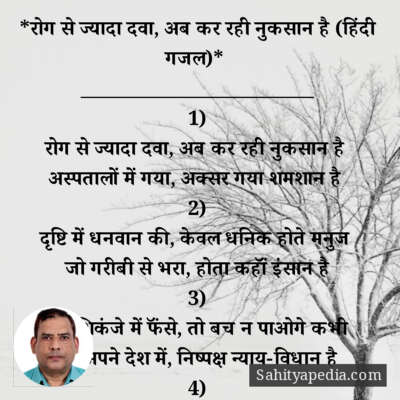ख्वाबों का कातिल
ख़्वाबों का कातिल ज़ब भी
रात अँधेरे आता है
ज्यों कुछ अच्छा दिखता है
झट से मुझे जगाता है
अपने मित्र भरम – चिंता को
मेरे हवाले कर देता है
भूख -प्यास में मुझे पिरोकर
हाथों से निवाला हर लेता है
अच्छा होने से नफ़रत उसको
अच्छाई का जानी दुश्मन
तोड़ देता है जीवन के
सपनों के घर को कण -कण
व्यथा व्यथित होकर कह देता
होता गर कोई सुनने वाला
गिरह पड़ी है धागे में प्रेम के
क्या ही करे कोई बुनने वाला
अच्छे ख़्वाबों की आवाजाही
पूर्ण चाँद की मधुर बेला में
उलझा हुआ मैं इक प्यादा हूँ
वक्त के शतरंजी खेला में
रंजिश करती हैं यादें
जिनमें वादों की जमात भी है
शब्द थे सो निकल गए
क्या अधरों की औकात भी है
सारे कलुष निरुत्तर प्रश्नों का
क्या कोई अब हल निकलेगा
आज तो धूमिल है बादल बन
क्या मौसम थोड़ा बदल निकलेगा
-सिद्धार्थ गोरखपुरी