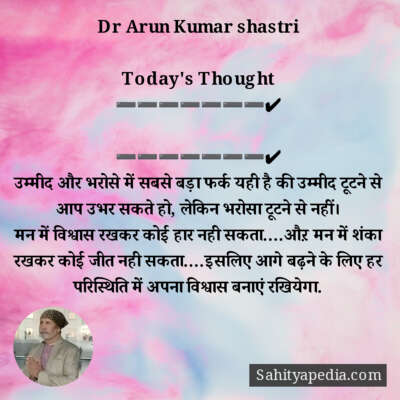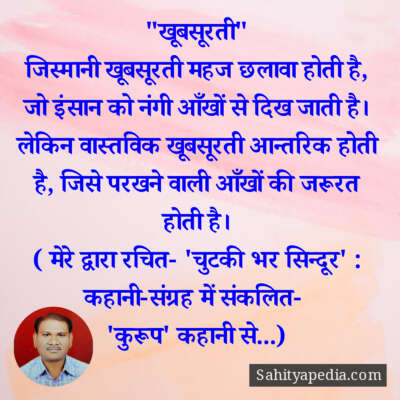किन्तु मेरे विजय की प्रथा
घण्टों बैठे मीलों दूर तक,
जीवन से मिलने,
बातें करने का
वक्त चाहिए,
कई सीमायें तोड़कर,
जीवन बाहर निकल चुका है
अपने हाथों से,
पहरों तक याद नहीं आती
अपने अस्तित्व की,
दिनों तक
अधर में लटकी सांसें,
गोया लौट नहीं पाती।
एक झरोखा धूप का जैसे,
जिन्दगी जीने का बहाना है
बादल घिरी दोपहरें,
अंधेरी शामें, काली रातें,
रोजाना सड़कों पर
प्रतीक्षा करती
अनगिनत अवश्यंभावी मौतें,
तैरते रहती हैं
काले गिद्द की तरह,
श्मसान छूती,
वापस लौट आती,
जिंदगी के आकाशों पर।
छिपकली की तरह
दीवार में चढ़ना,
फि़र गिर जाना,
बिना खूंटी के उंगलियां
पत्थरों में रोपे,
कितनी बार
इन जानलेवा चट्टानों की
श्रेणियां चढ़ी हैं मैंने,
कितनी बार
मैंने जलाई होंगी,
बुझती हुई चिंगारी से
नई आग।
कितने दूर तक गया हूं मैं,
अपने कंधों पर
इलाके भर के उम्मीदों की,
जिन्दा लाशें लटकाये,
कितने बयांबे,
कितने बीहड़,
बंजर, निर्जन,
रेगिस्तानों की जलती छाप है,
मेरे तलुवों में,
जीवन के उपक्रमों की
तलाश में,
जैसे जीवन का उपहास हो गया।
इस संग्राम की परिणति क्या होगी
मुझे नहीं मालूम,
इस संघर्ष की उपलब्धि क्या होगी,
मुझे नहीं मालूम,
किन्तु मेरे संस्कारों को
खूब सिखाया गया कि ,
सुबह की प्रतीक्षा करना मेरा धर्म है,
और संघर्ष करना मेरा कर्म है,
मैं न शाश्वत हूं, न अनश्वर,
किन्तु मेरे विजय की प्रथा,
शाश्वत थी, शाश्वत रहेगी।
-✍श्रीधर.