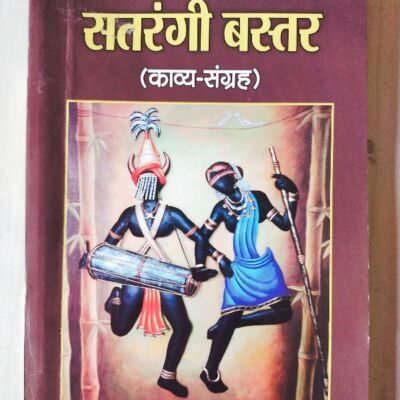काश
मैं फिर यही कहूँगी
और हर बार कहूँगी
कि मुझे कोई दस्तक़
अब सुनाई नहीं देती
मैंने ख़ुद ही उसके
इंतज़ार में वक़्त गवाया है
और उसकी हरेक
दस्तक़ पर
अपने कानों पर रखके हाथ
उस दस्तक़ की गूंज को
हर बार दबाया है
कल्पनाओं से भर
मैंने उसके चित्र बनाकर
जिया और अपने हाथों से
उन्हें फिर मिटाया है
उसके शब्दों और ख़यालात
को लेकर ही मैंने
एक खवाबों का पूरा जहान
कहीं मन में बसाया था
फिर उसी के शब्दों ने
उसे मिटटी में मिलाया है
होती रही गुफ़्तगू मेरी
सालों तलक़ ख़ुद से खुद ही में
और हर गुफ़्तगू के बाद
मैंने ख़ुद को एक अवसाद में पाया
अवसाद में अक़्सर अब “शायद”
और “काश” ही मेरे हिस्से में आया
एक तयशुदा वक़्त पर
दम तोड़ते हैं रिश्ते
कुछ इस तरह ही अपनी
अधूरी सी कहानी ने भी
अंतहीन समाप्त ही पाया है।
किरण वर्मा