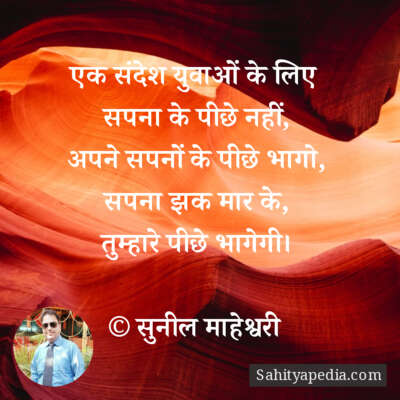एक लब्ज ‘मां’
एक लब्ज ‘माँ’
जब भी “मां” मुझे बुलाती है,
फिजायें दौड़ी चली आती है।
नर्म शाखों की शबनमी बूँद छू लूँ,
माँ उंगली पकड़ चलना सिखाती है।
आज भी लगाकर नज़र का टीका
मां मुझे चश्म-ए-बद से बचाती है।
थपकी के लिए बेताब जिद्दी दिल,
मां मेरी अब भी लोरी सुनाती है।
जरा खुश्क भी हुई तो क्या हुआ,
मां के हाथों की रोटी बड़ी भाती है।
कहां गुमहुई धानी चुनर की खुशबू,
क्यो हवायें अब साथ नही लाती है?
हाल क्या सुनाये अहल-ए-महफिल में
मेरी तबियत का राज नज़र बताती है।
मेरी कलम जब भी आदाब करना चाहे,
आहिस्ता एक लब्ज ‘मां’ लिख जाती है।
Rishikant Rao Shikhare
24-06-2019