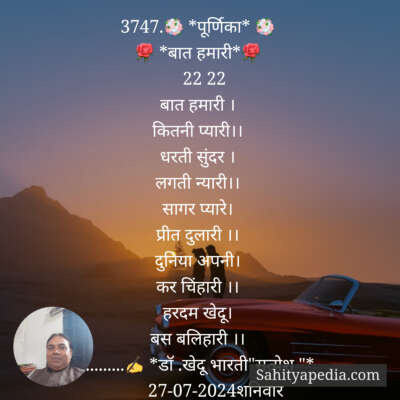बूढ़ी सांसें (कविता) – मोहित नेगी मुंतज़िर
बूढ़ी सांसें चल रही थीं
सहारे लाठी के
मैं हथप्रभ था
झुका हुआ था शर्म से
और सोचता था
काश!
मैं कुछ कर पता…
मगर अफ़सोस!
इंसानियत की हुई हार…
सिवाय सोचने के
कुछ कर न पाया मैं!
उस कंपकंपाते बदन को देखकर
हो रहा था प्रतीत
मानो डोल रही हो धरती
और कांप रहा हो आकाश!
देखता रहा स्थिर, अविचल,
हताश, उदास, शोकपूर्ण
गंभीर नज़रों से
क्या है जीवन??
आखिर इतनी असमता क्यों??
आखिर दुख का प्राकटय
इतना निर्मम भी होता है??
क्यों सूख जाते हैं
अपनेपन के स्रोत??
क्यों नदी सा उफ़ान भरता जीवन
कहीं लुप्त हो जाता है…
क्या जीजिविषा हो जाती है कम??
या रूठ जाती है किस्मत??
वो चलता रहा सड़क पर
एक निडर पथिक-सा
आज देखता हूँ
कि हाथ फैला लेता है वह
हर किसी के सामने
क्या न रहा होगा स्वाभिमान
जीवन में उसके??
या केवल ज़िन्दगी जीना ही
अब उसका स्वाभिमान बन गया है।
©मोहित नेगी मुंतज़िर