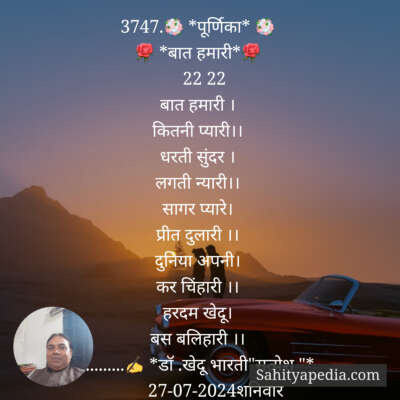दिन बचपन के
मुझे याद आया अपना बचपन,
दर्पण में जब देखा प्रतिबिम्ब।
कहा आईने से इस बड़प्पन की मूरत को,
तू ही संभाल न कर विलम्ब।
मैं दौड़ चली अपने बचपन में।
बचपन की वो गलियां,
सारी सखियों का घेरा।
वो खेलों का खतम न होना,
चाहे हो जाए अंधेरा।
रेतों में पांव घुसा कर,
घर छोटे छोटे बनाना।
लगता था सारी दुनिया को,
इसके अंदर है बसाना।
वो पकड़म पकड़ाई,
वो खो-खो खेल सुहाना।
वो घर-घर का खेल खेलना,
गुड़ियों के ब्याह रचाना।
मम्मी से आंख बचाकर,
पुराने कपड़ों को बिखराना।
नित नये-नये स्वांग रचाना,
बदले में इसके तो था,
पक्का ही डांटें खाना।
फिर रूठ कर पड़ जाना,
मांँ को नखरे दिखलाना।
मुझको तो भूख नहीं है,
आ रही है नींद मुझे तो।
फिर प्यारी माँ को खिझाना,
सौ सौ मनुहार कराकर।
झूठे नाटक दिखलाना।
मांँ की ममता को बिल्कुल,
मोम सा नरम पिघलाना।
फिर हंस कर झट उठ जाना,
मांँ से जा लिपट जाना।
सौ सौ बलैंया ले कर,
वो माँ का प्यार जताना।
अब कहां वो गुजरा जमाना।
पर लाख भुलाना चाहूं,
आंखों से न होता ओझल,
वो गुजरा हुआ जमाना।
वो बीता हुआ फसाना।
फिर लौट आई उस अक्स में,
वही बड़प्पन की मूरत।
जिसको कि निभाना सब कुछ,
इन्कार की नहीं कोई सूरत।
—रंजना माथुर
दिनांक 29/08/2017 को
मेरी स्व रचित व मौलिक रचना
@copyright