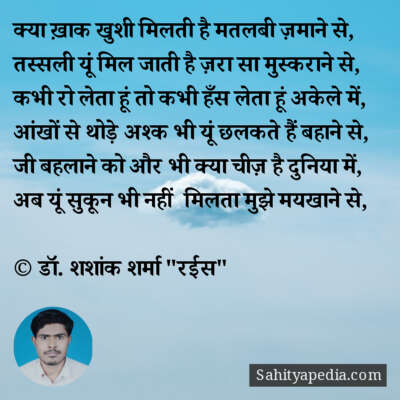क्षणिकाऐं
(1)
उदास धूप की परतों पर
आसमां की चमक सो रही है
सूरज डरा सा मिला,
चाँद सुस्त सोया है
जनतंत्र के बादल बहुत हैं
मगर बारिश की बूँदें नहीं,
प्रगति का शोर कर्णभेदी,
आम और खास के बीच,
गहराती खाई में गूंजता,
गरीब की भूख प्यास बढ़ती
अमीर की हवस बढ़ती
कानून की किताबों में
यही लोकशाही हुई।
आवारा पशुओं का हिसाब
दीमकों चींटियों की गिनती
आसान है लेकिन
आदमी की गणना
बहुत दुष्कर, असंभव है
पैदाइशें थामने में
कंगाली आड़े आ जाती
ज्यों ज्यों गरीबों की
कोख भरती
त्यों त्यों भुखमरी दरिद्रता
दामन से आकर बस जाती
कहीं धर्म, कहीं समाज
आड़े आता और
पैदाइश का चक्रव्यूह
रुक नहीं पाता
रोकना टोकना नहीं है
यह भारत है चीन नहीं है
महान हैं हम,
आम नहीं हैं
मनमर्जी से चीखो चिल्लाओ
रास्ते जाम करो
सरकारें चुनो
फिर उन्हें नाकाम करो
अपने हाथ पे हाथ धरे
गप्पें मारो
बड़ी बड़ी बेअर्थ बेहिसाब हांको
सुना कानून की किताबों में
यही लोकशाही हुई।
(2)
जेब खाली
चौका चूल्हा
संदूक खाली
घर खाली है
रिश्ते नाते खूब हैं मगर
अपनेपन की कंगाली है
यारी दोस्ती के मायने
यों समझ में आया
कि
मां-बहन की गालियों में
अपनेपन की बोली है
मगर
दाल रोटी नमक के लिए
आपसी पेंचा लेना देना
अपनेपन की निशानी नहीं,
अब के ‘सभ्य समाज’ में
बहुत भद्दी गाली है।
-✍श्रीधर.