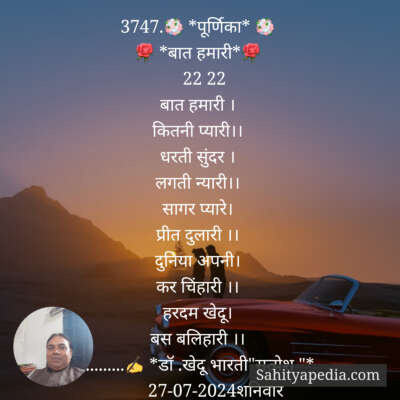कवि एवं वासंतिक ऋतु छवि / मुसाफ़िर बैठा
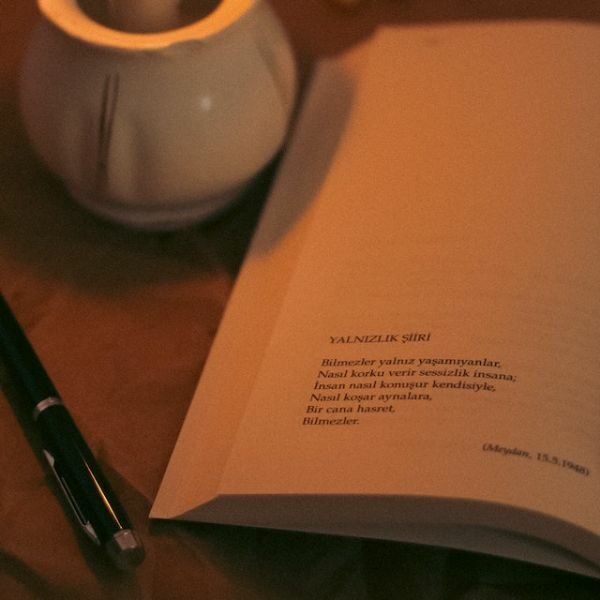
कवियों ने बसंत के गीत असंख्य गढ़े हैं।
पढ़े हैं कसीदे निर्बंध अनंत उसके
की हैं कसरतें तमाम सुख शांति आह्लाद
ढूँढ पा लेने की महज इसी मौसम में
मानो अन्य तमाम ऋतुओं को
इसकी सरदारी में लताड़ लगाना जरूरी हो
किसी ने वीरों का बसंत ढूंढा
किसी ने कविता में बसंती हवा का मानवीकरण कर
उसको अनोखी और न जाने क्या क्या बता डाला
किसी ने प्यार प्रेम की पेंगें बसंत में ही बढ़ाने की कड़ियाँ जोड़ीं
जैसे पंडित पतरा से बांधते हैं दिन
नागरी ललनाओं ने बसंत को क्लबों होटलों की पार्टियों में बाजबरर्दस्ती पटक पहुँचाया
इस ऋतु को अलग से दुलारा सहलाया गया नाहक और दूजे से सौतेला किया गया व्यवहार
वर्षा जैसी जीवनदायिनी ऋतु को भी कवियों ने
इसके आगे न दिया मान
जैसे कि हरियाली की नींव धरने वाली
बसंत को कोख देने वाली इस ऋतु से
कवि नातेदारी की कोई जरूरत ही न हो।
बसंत को पुरुष कवियों ने अपनी सुविधा एवं मर्द नजरों से देखा
सावन को तरह तरह से झुमाया
युवा नारी देह की सोलह को सावन से लगाया
गोया मर्द देह को सावन से समझा ही नहीं जा सकता
ऋतुओं से जो दो चार नहीं करते
होते हों साफ़ अनभिज्ञ
होटलों क्लबों में वे सावन और बसंत के गीत गाते हैं
जबकि दो जून की रोटी को संघर्षरत मजदूरों का, आम जनों का
न तो कोई सावन होता है न भादो
बसंत तो अलग से बिलकुल ही नहीं
सावन का अँधा भले ही न होता आया हो कवि
पर बसंत और सावन की अंधभक्ति आरती में तो
भेड़ियाधसान उतरता रहा ही है कवि!
–