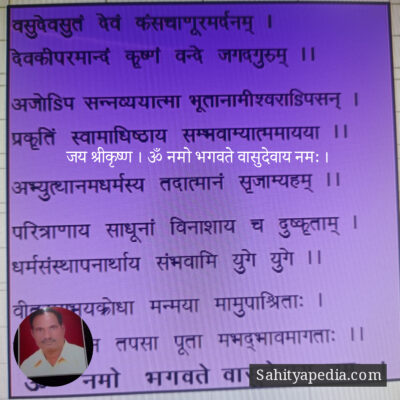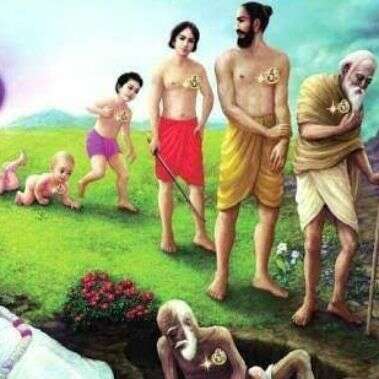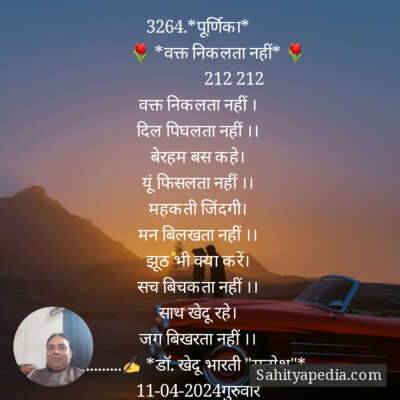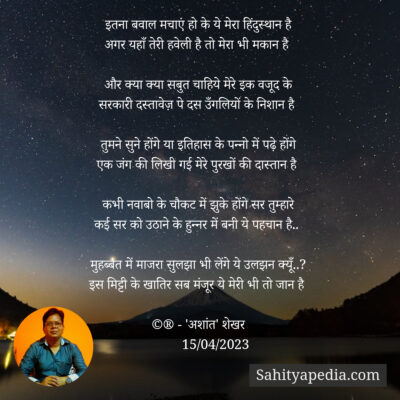हिन्दी ग़ज़लः सवाल सार्थकता का? +रमेशराज

ग़ज़ल अपनी सारी शर्तों, ;कथ्य अर्थात् आत्मरूप-प्रणयात्मकता तथा शिल्परूप- बह्र, मतला, मक्ता, अन्त्यानुप्रासिक व्यवस्था में रदीफ काफिये, अन्य तकनीकी पक्ष जैसे शे’रों की निश्चित संख्या, हर शे’र का कथ्य अपने आप में पूर्णता ग्रहण किए हुए आदि-आदि के साथ ही लिखी जानी चाहिए। चाहे उसका सृजन हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली या उर्दू में हो, लेकिन पुकारी या कही जानी ग़ज़ल ही चाहिए। ग़ज़ल अपनी सारी शर्तों को पूर्ण किए बिना अपने अस्तित्व या चरित्र की रक्षा कैसे कर पायेगी या किस तरह ग़ज़ल कहलाएगी? बहस का मुख्य बिन्दु यही होना चाहिए। किसी वस्तु को परम्परा से काटकर उसका मूल्यांकन उसी परम्परा में करना अतर्कसंगत ही माना जाना चाहिए। होली के अवसर पर दीप जलाकर, लक्ष्मी का पूजन एवं पटाखे छोड़कर क्या हम होली की परम्परा को जीवित रख सकते हैं? या ऐसी परम्परा को ‘होली’ नाम से पुकार सकते हैं? जनसमूह तो नेताओं की सभाओं में भी होता है। वहाँ खाने-पीने से लेकर तरह-तरह के मनोरंजन की दुकानें भी लगाई जाती हैं। क्या इस प्रकार के एक राजनीति मंच को किसी मेले के रूप में पहचाना जा सकता है? हर स्थिति में एक विवेकशील मनुष्य इसका उत्तर ‘न’ में ही देगा। अपनी परम्परा, अपनी शर्तों से कटकर कोई वस्तु उसी परम्परा के साथ जीवित या सार्थक रह ही नहीं सकती है।
लेकिन ग़ज़ल के साथ यह कमाल या चमत्कार कम से कम हिन्दी में तो हो ही रहा है। ‘प्रसंगवश’ के ‘समकालीन हिन्दी ग़ज़ल विशेषांक फर.-1994’ में डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी का आलेख ‘आधुनिक हिन्दी ग़ज़लः रचना और विचार’ ग़ज़ल को ग़ज़ल की परम्परा या शर्तों से काटकर हिन्दी में ग़ज़ल कहलवाने अथवा मनवाने का एक ऐसा मायाजाल है जो किसी सार्थक हल की ओर पहुँचाता तो कम है, भटकाता ज्यादा है। डॉ. सत्यप्रेमी अपने मत के पक्ष में विभिन्न विद्वानों के अभिमत प्रस्तुत करते हुए यह कहकर भले ही आश्वस्त हो लें कि ‘‘ग़ज़ल की विषयवस्तु को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं और यह मतभेद ही ग़ज़ल के उर्दू ग़ज़ल और हिन्दी ग़ज़ल नामकरण की पृष्ठभूमि भी निर्मित करता है’’, लेकिन यह आश्वस्ति दीर्घकालिक या स्थायी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हीं के अनुसार विद्वानों में मतभेद हैं और हमारे हिसाब से आगे भी इसलिए रहेंगे क्योंकि इसका हमारे पास न तो कोई शास्त्रीय हल है और न हम किसी शास्त्रीय तरीके से इस मुद्दे को हल करना चाहते हैं। नीम को बबूल या बबूल को नीम मनवाने की यह जोर-जबरदस्ती मतभेदों को नहीं तो किसको जन्म देगी?
उक्त आलेख पर अगर हम [ विभिन्न विद्वानों के अभिमतों को डॉ. सत्यप्रेमी के मतों से मिलाते हुए ] क्रमशः अध्ययन, चिन्तन, मनन करें तो जिन मतभेदों की काली छाया से डॉ. सत्यप्रेमी शुरू से ही आतंकित होते हैं, वह काली छाया इस आलेख के अन्त में भी ज्यों की त्यों मौजूद रहती है। डॉ. सत्यप्रेमी फरमाते हैं कि-‘‘एस.एन. अहमद फारुख ने अपने लेख ‘हिन्दी उर्दू ग़ज़ल का स्वर [ युगधर्म, दीपावली विशेषांक-1978 ] में लिखा है कि ‘‘ग़ज़ल की यह विधा जब हिन्दी साहित्य में प्रवेश करती है…. तो इसके एक-एक शब्द से देशभक्ति, इन्सानी दर्द और कौमी बेदारी राष्ट्रीय [ चेतना ] टपकती-सी प्रतीत होती है।’’
अब डॉ. सत्यप्रेमी और एस.एन. अहमद फारुख साहब को यह तो कोई भाषा वैज्ञानिक ही समझा सकता है कि उर्दू और हिन्दी दो अलग-अलग भाषाएँ नहीं हैं, बल्कि उर्दू, हिन्दी की एक बोलीमात्र या हिन्दी ही है और इस भाषा वैज्ञानिक सत्य या वास्तविकता के कारण हिन्दी और उर्दू की यह सारी बहस ही अपने-आप बेमानी या खारिज हो जाती है।
बात आती है-ग़ज़ल के हिन्दी में इस तरह प्रवेश करने या कराने की, तो फारुख साहब से यह तो पूछा ही जा सकता है कि क्या वे ग़ज़ल की तर्ज पर ही हज़्ल को भी इसी तरह, हिन्दी में प्रवेश दिला सकते हैं, जिस तरह उन्होंने ग़ज़ल को हिन्दी में साकी, शराब मयखाने से मुक्ति दिलायी है।
खैर… इस तरह हज़्ल भी हिन्दी में आकर अपनी अश्लीलता से कुछ तो मुक्ति पायेगी। पर सोचना यह है कि ऐसे में हज़्ल कैसे हज़्ल कहलायेगी? हिन्दी और उर्दू के छद्म भेद पर टिका यह चिन्तन, निष्कर्ष के किसी पड़ाव तक इसलिये नहीं ले जा सकता है क्योंकि इसकी सारी की सारी प्रक्रिया अपाहिज होने के साथ-साथ जिधर मंजिल है या होनी चाहिए, ठीक उसके विपरीत दिशा में हाथ-पैर पटक रही है।
इसी आलेख में डॉ. सत्यप्रेमी, डॉ. जानकी प्रसाद के विचारों से इस तथ्य की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं कि ‘‘वर्तमान समय में उर्दू भाषा का व्यवहार करने वाली जाति अखण्ड भारत का हिस्सा बन गयी है। ऐसी स्थिति में उर्दू भाषा के शब्द भी हिन्दी भाषा में अपनी मूल प्रकृति खोकर प्रयुक्त होते हैं तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ग़ज़ल को हिन्दी कविता में उर्दू फारसी कविता की समीपता तथा भारतीय और इस्लाम संस्कृतियों के साहचर्य के संदर्भ में ग्रहण किया है। ग़ज़ल का हिन्दी में आगमन, एक साहित्यिक घटना ही नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना भी है।’’
डॉ. सत्यप्रेमी के अनुसार जब स्थिति यह है कि यह सांस्कृतिक मेलमिलाप अपने स्वाभाविक प्रक्रिया को अपना रहा है, भाषा की दृष्टि से उर्दू और हिन्दी अभिन्न बनने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, तब ग़ज़ल की दृष्टि से हिन्दी और उर्दू के भेद और क्यों गहराते जा रहे हैं? स्वाभाविकता में पैदा की गयी यह अस्वाभाविकता मतभेदों को नहीं तो किसको जन्म देगी। ग़ज़ल विभिन्न सांस्कृतिक एवं भाषिक मेलमिलाप जैसे अरबी-फारसी, उर्दू आदि के बीच ग़ज़ल ही रही लेकिन हिन्दी के साथ तालमेल बिठाने में उसे ऐसी दिक्कतों या झगड़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है जैसी कि दिक्कतें या झगड़े धर्म के नाम पर सम्प्रदाय पैदा कर देते हैं या कर रहे हैं। ऐसे मतभेदों को स्वीकारते हुए भी, इन्हीं मतभेदों को ऐसे आलेखों के माध्यम से और गहराते जाना कौन-सी समझदारी है?
जब सारा का सारा विवेचन कुतर्कों और अवैज्ञानिक सूझबूझ के सहारे चल रहा है तो डॉ. सत्यप्रेमी का इस प्रकार खीज उठना भी समझ से परे है कि ‘‘ इतना सब कुछ स्पष्ट हो जाने के पश्चात भी हिन्दी के स्वनामध्न्य आलोचक-समीक्षक विद्वान हिन्दी ग़ज़ल को आधुनिक युग की एक सशक्त विधा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हिन्दी ग़ज़ल की पर आये दिन प्रहार करते ही रहते हैं।’’
जिसे डॉ. सत्यप्रेमी ‘इतना कुछ स्पष्ट’ कह रहे हैं उसमें ‘थोड़ा-सा ही ‘कुछ’ स्पष्ट हो जाता तो उन्हें यह ‘सब कुछ’ न कहना पड़ता और इस विरोध को अपने कुतर्कों के सहारे पूरी की पूरी भारतीय आलोचना/ समीक्षा के माथे पर कलंक के टीके की तरह नहीं मढ़ना पढ़ता? चाहे वे इस बात की लाख दुहाई दें कि-‘‘वास्तविक मूल्यांकन के साहसिक तथा यथार्थपरक दृष्टिकोण के अभाव में प्रत्येक सही कृति समीक्षकों के दायरे में कविता के सामान्य महत्व से भी वंचित रही। कबीर, भारतेन्दु, निराला, मुक्तिवोध, राजकमल चैध्री, धूमिल, दुष्यंत कुमार, अनिल कुमार तथा आज की कविता-अकविता के साथ यह दुर्घटना घटी।’’
इन सब बातों का उत्तर सिर्फ यह है कि यदि रचनाओं का धरातल ठोस, वास्तविक, शास्त्रीय और सत्योन्मुखी है तो आज नहीं तो कल उनका जादू सर पर चढ़कर बोलेगा ही। उपरोक्त नाम घने झंझाबातों के बावजूद आज भी प्रासंगिक हैं। जिन लचर और कमजोर रचनाओं ने जन-कविता का कभी भी गौरव पाया है तो आगे चलकर खोया भी है। इसलिये चिंता का विषय यह नहीं। चिन्ता तो यह है कि जब ‘नासमझी’ समझदारी का रूप ग्रहण कर ले, ‘तर्कहीनता’ तर्क बनने का प्रयास करे तो क्या किया जाये? जब तर्क के नाम पर ऐसे कुतर्क देकर किसी सार्थक मूल्यांकन की दुहाई दी जाये कि-‘‘पूर्व निर्धारित नियमों एवं उपनियमों को टटोलने से कविता की सच्चाई नहीं पायी जा सकती?’’
डॉ. सत्यप्रेमी ऐसा कहकर क्या संकेत देना चाहते हैं? सच पूछा जाये तो उनके या उन जैसे हिन्दी ग़ज़ल के पक्षधरों की कलई इसी बिन्दु पर आकर घुल जाती है। दरअसल ऐसे हिन्दीग़ज़ल के पक्षधर या विद्वान ग़ज़ल के नाम पर पाठकों को ऐसा बूड़ा-कचरा परोसना चाहते हैं, जिसे हिन्दी साहित्यकारों को आँख मूँदकर उनके गले उतारा जा सके। इसके पीछे छुपा स्वार्थ भानु प्रताप सिंह ‘भानु’ के शब्दों से पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है कि-‘‘उर्दू ग़ज़ल का ज्यों का त्यों अनुकरण हिन्दी कवियों को सफलता नहीं दे सकेगा। उर्दूग़ज़ल से भिन्नता होनी ही चाहिए अन्यथा हिन्दी और उर्दू ग़ज़ल में एक रूप होने से हिन्दीग़ज़ल का अस्तित्व पृथक् न रहेगा। दोनों भाषाओं की ग़ज़लों में एक विभाजन रेखा होना अत्यावश्यक है।’’
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, श्री एस.एन. अहमद फारुख और श्री भानुप्रताप सिंह ‘भानु’ के इन निष्कर्षों के आधार पर आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग़ज़ल के नाम पर एक बहुत बड़ी खाई हिन्दी और उर्दू के बीच खोदी जानी आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक है। ऐसा करने पर ही हिन्दी ग़ज़ल का अस्तित्व कायम किया जा सकता है। हिन्दी में ग़ज़ल के अस्तित्व की रक्षा के लिये भले ही ग़ज़ल के चरित्र अर्थात आत्मा और शरीर [ नियम-उपनियम ] अर्थात् शिल्प की हत्या करनी पड़े, हिन्दी के ऐसे विद्वान ऐसा करने में चूकेंगे नहीं। ग़ज़ल की हत्या कर ग़ज़ल को प्राणवान घोषित करने की यह प्रक्रिया कितनी सार्थक और सारगर्भित है? इसका अनुमान बड़ी ही सहजता से लगाया जा सकता है। सच तो ये है कि हिन्दी ग़ज़ल के पक्ष में डॉ. सत्यप्रेमी का उक्त आलेख निर्जीव और आधारहीन सिद्धान्तों और तर्कों के सहारे खड़ा होने का प्रयास करता है। और यही वजह है कि अपनी लाख कोशिशों के बावजूद औंधे मुँह गिर पड़ता है। डॉ. सत्यप्रेमी लिखते हैं कि-‘‘ समकालीन हिन्दी ग़ज़ल पारम्परिक ग़ज़ल की काव्य रूढि़यों से मुक्त होने का प्रयास भी है तथा नये शिल्प एवं विषय का विकास भी इसमें परिलक्षित होता है।’’
डॉ. सत्यप्रेमी ने अगर थोड़े से तर्कों का भी सहारा लिया होता तो सबसे पहले परम्परागत ग़ज़ल की काव्य-रूढि़यों को बतलाते और इसके उपरांत हिंदी ग़ज़ल के उत्तरोत्तर विकास को समझाते। इस प्रकार परंपरागत ग़ज़ल की काव्य-रूढि़यों से मुक्ति पाने के प्रयास को पाठक आसानी से समझ लेते। लेकिन उन्होंने यह सब कुछ न समझाते हुए इन सवालों से पलायन करने में ही अपने समझदारी का परिचय दिया है। यह पलायन की प्रवृत्ति उन पर किस तरह हावी है इसका एक उदाहरण और प्रस्तुत है-
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी फरमाते हैं-‘‘ हिन्दी ग़ज़ल के नामाकरण को लेकर भी इन दिनों विवाद की स्थिति निर्मित हो गयी है। डॉ. धनंजय वर्मा और डॉ. राजेन्द्र कुमार ने धर्मयुग ,16 नवम्बर 1980 में हिन्दी ग़ज़ल की सकारात्मक दृष्टि को कुंठित किया है और उर्दू और हिन्दी की भाषायी मामले को रेखांकित किया है। डॉ. राजेन्द्र कुमार ने हिन्दी ग़ज़ल की सार्थकता एवं औचित्य को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से प्रतिपादित किया है।’’
यहाँ गौरतलब बात यह है कि डॉ. सत्यप्रेमी ने डॉ. वर्मा की बात को बिना कोई तर्क दिये हवा में उड़ाने की कोशिश की है। अगर डॉ. वर्मा को हिन्दी ग़ज़ल में साम्प्रदायिक बू महसूस हुई और उन्होंने हिन्दीग़ज़ल की सकारात्मक दृष्टि को कुंठित किया तो सत्यप्रेमी को यहाँ उनका पक्ष रखते हुए यह जरूर बताना चाहिए था कि हिन्दीग़ज़ल में ‘इन प्रमाणों’ के साथ कहा जा सकता है कि हिंदी ग़ज़ल में कोई साम्प्रदायिक बू नहीं है और डॉ. वर्मा ने ऐसे किया है हिन्दी ग़ज़ल की सकारात्मक दृष्टि को कुंठित। इसके साथ ही वह यह बताते कि हिन्दी ग़ज़ल की सकारात्मक दृष्टि क्या है? इन सब सवालों के जवाब न देकर, उन्होंने सीधे और सरल रास्ता इन सवालों से पलायन का अपनाते हुए डा. वर्मा की बात पाठकों या सुधीजनों की समक्ष न रखी। डॉ. राजेन्द्र कुमार के तथ्यों को ही सबके समक्ष रखने में अपनी वाहवाही समझी।’
डा. राजेन्द्र कुमार अपने लेख ‘हिन्दी ग़ज़ल कहना ही होगा’ में तर्क देते हैं-‘‘ अगर कोई ग़ज़ल को अपनी निजी परम्परा और निजी प्रतीकात्मक व्यंजना के नाम पर उसमें गुलो-बुलबुल, शमा-परवाना को यथावत बनाये रखने का हिमायती हो तब तो बेशक हिन्दी ग़ज़ल इस बात की गुनहगार है कि उसने इस परम्परा से हटकर अपने प्रयोग किये हैं लेकिन यह कहना कि ग़ज़ल की असली शक्ति तो उसकी कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता में है, उसे ही ग़ज़लों ने छोड़ दिया है, ठीक नहीं है। छोड़ा है तो काल्पनिकता को छोड़ा है, कल्पनाशीलता को नहीं। अफसोस है कि कुछ लोग काल्पनिकता और कल्पनाशीलता के अंतर को, एक के मुकाबल दूसरे की महत्ता को महसूस करने से कतराते हैं। इसीलिये उन्हें ग़ज़ल की मूल प्रवृत्ति पर आघात होता नजर आता है।’’
अगर हम परम्परागत ग़ज़ल का ही विवेचन करें तो उसमें गुलो-बुलबुल, शमा-परवाना, साकी-शराब-मयखाना अपने अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक या प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इसके अतिरिक्त भाषायी-विस्तार न हुआ हो, ऐसा कहना, सोचना, समझना, परम्परागत ग़ज़ल की परम्परा पर आँख मूँदकर बयान देने के अलावा कुछ नहीं। परम्परागत ग़ज़ल में वह सबकुछ भाषायी स्तर पर मौजूद है, जिसकी दुहाई परम्परागत ग़ज़ल को खारिज कर हिन्दीग़ज़ल की स्थापना को लालायित आज हिन्दी ग़ज़ल के पुरोधा दे रहे हैं। साथ ही यह बात भी दावे के साथ नहीं कहीं जा सकती है कि हिन्दी ग़ज़ल शमा परवाना, साकी-शराब, मयखाना, गुलो-बुलबुल से मुक्त हो गयी है। यदि इनके स्थान पर फूल, तितली, शलभ-लौ, मदिरा, मदिरालय, मेंहदी, अधर , चुम्बन, यौवन आदि ने ग्रहण कर भी लिया है तो यह कोई बहादुरी का कार्य इसलिये नहीं है क्योंकि इससे परम्परागत ग़ज़ल की न तो परम्परा टूट गयी है और न हिन्दी ग़ज़ल ने नये प्रतिमान स्थापित कर लिये हैं। बल्कि इससे तो परम्परा को हर प्रकार विस्तार ही मिला है। इस विस्तार को यदि हिन्दी ग़ज़ल कहकर प्रचारित किया जायेगा तो सोचना यह पड़ेगा कि उर्दू ग़ज़ल [ जिसे खुद हिन्दी वाले उछाल रहे हैं, उर्दू वाले नहीं ] क्या है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तो उर्दू हिन्दी है’ ऐसे में हिन्दी-उर्दू का यह विवाद ग़ज़ल का विवाद न होकर भाषायी विवाद ज्यादा है। अगर भाषायी विवाद के आधार पर ही हमें विधाएँ या साहित्य को तय करना है, वह भी अवैज्ञानिक तरीके से, तो हम ऐसे आदरणीय विद्वानों से एक सवाल जरूर-यदि संज्ञा या संज्ञा विशेषणों मात्र के आधार पर ही कोई भाषा अपना भाषिक आधार खड़ा कर लेती है, भाषा के लिये यदि शब्दावली ही प्रमुख है तो हिन्दी में रेल, इन्जन, पिन, आलपिन, जंगल, टायर, ट्यूब, पंचर, बल्ब, होल्डर, साईकिल, स्टेशन आदि का विकल्प क्या है? ऐसे शब्दों का हिन्दी के सर्वनामों, क्रियाओं आदि के साथ बहुतायत से प्रयोग करने पर क्या ग़ज़ल हिन्दी की जगह ‘अंग्रेजी ग़ज़ल’ हो जायेगी?
बात आती है इन्हीं शब्दों के प्रतीकात्मक, व्यंजनात्मक प्रयोग के संदर्भ में तो डॉ. राजेन्द्र कुमार का यह कथन कि-‘‘ परम्परागत ग़ज़लें शमा-परवाना, गुलो-बुलबुल तक ही सीमित रही हैं और हिन्दी ग़ज़ल इस सीमा को तोड़कर बाहर खड़ी है?’’ यह धारणा ग़लत इसलिये है क्योंकि ग़ज़ल के इस प्रणयात्मक रूप का हिन्दी में आज भी प्रचलन खूब जोरों पर है। ज्यादा दूर न जायें तो इसका प्रमाण पंकज उदास, अनूप जलोटा जैसे ग़ज़ल-गायकों और सरिता, सुषमा आदि में छपने वाली गजलों तथा स्वयं ‘प्रसंगवश’ का यह हिन्दी ग़ज़ल विशेषांक इसका प्रमाण है। यह तो डॉ. राजेन्द्र कुमार खुद स्वीकारते हैं कि ग़ज़ल की तरह हिन्दीग़ज़ल में भी प्रतीकात्मकता और कल्पनाशीलता के तत्व विद्यमान हैं, बस छोड़ा है तो काल्पनिकता को। प्रश्न यह है कि हिन्दी में जो ग़ज़लें लिखी जा रही हैं, जब तक उनमें रूमानी संस्कार विद्यमान हैं, तब तक यह दावे के साथ कैसे कहा जा सकता है कि उसने काल्पनिकता से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है?
अगर यह मान भी लिया जाये कि ग़ज़ल हिन्दी में आकर अपने परम्परागत संस्कारों से कटकर गुलो-बुलबुल की दास्तान नहीं रही है। डॉ. सत्यप्रेमी के अनुसार ‘अब इसमें अनास्था, निराशा, ऊब के साथ-साथ आक्रोश, विद्रोह और प्रतिकार के स्वर मुखर हो रहे हैं।’’
डॉ. महावीर के मत से-‘‘इसका सम्बन्ध इश्क और व्यक्तिगत भावों में न होकर सामाजिक जीवन की विसंगतियों से है।’’
प्रो.वी.एल. आच्छा की नजर में-‘‘हिन्दी ग़ज़ल ने उस मुहावरे को पकड़ने की पहल की है, जिसके केन्द्र में समकालीन जीवन के दर्दीले परिदृश्य हैं।’’
इन सब बातों का औचित्य तभी सिद्ध किया जा सकता है, जबकि मूल कृति और उसका चरित्र क्या है और परिवर्तन के बाद उस मूल कृति ने जो नया रूप या चरित्र ग्रहण किया है उसके अनुरूप उसका परम्परागत नाम या विशेषण उसे सार्थकता प्रदान करता है, अथवा नहीं? इस संदर्भ में अगर ग़ज़ल ने हिन्दी में आकर अपने परम्परावादी चरित्र को त्याग दिया है, वह साकी, प्रेयसी, नृत्यांगना [ कुल मिलाकर एक भोगविलासी औरत ] की जगह अब ऐसी औरत की भूमिका निभा रही है, जिसे हर प्रकार से राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक दायित्वों का बोध है, तब प्रश्न यह है कि क्या हम उसे अब भी ‘भोगविलासी औरत’ कहकर पुकारें या इस चरित्र के अनुरूप उसे कोई नया नाम दें? इसी केन्द्र बिन्दु से इसी केन्द्र बिन्दु तक सारी की सारी बहस शुरू की जानी चाहिये। बहस के इस बिन्दु पर आकर हिन्दी ग़ज़ल के प्रवर्तकों , उद्घोषकों, पक्षधरों की सारी की सारी चिन्तनप्रक्रिया को लकवा क्यों मार जाता है? हिन्दी ग़ज़ल का राग अलापने वाले जब तक इस तरह की बहस में शरीक नहीं होंगे, तब तक ग़ज़ल में न तो हिन्दी तय की जा सकेगी और न हिन्दी में ग़ज़ल।
———————————————————
रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ-202001